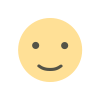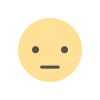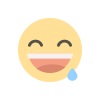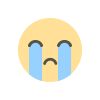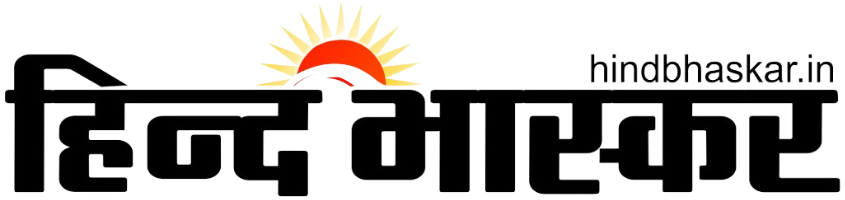होली: एक लोक पर्व; बदलता कलेवर: आचार्य ओमप्रकाश मणि
समाज की जीवन्तता का प्रमाण उसकी परिवर्तनशीलता में निहित है।

समय परिवर्तन शील है। समाज की जीवन्तता का प्रमाण ही उसकी परिवर्तनशीलता में निहित है।अपरिवर्तनशील समाज मृत प्राय होता है।पर कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमें निराशा के गहन आवर्त में ढकेल ले जाते हैं। यद्यपि कि मेरे सबसे प्रिय गद्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अभिमत है कि समाज के बदलाव पर निराश नहीं होना चाहिए। परन्तु मैं उनके जैसा स्थिति प्रज्ञ दार्शनिक नहीं हूं। मैं निराश होता हूं। भारतीय लोकपर्वों पर बदलते सामाजिक परिदृश्य मुझे निराश कर देते हैं।
आज होली है।रात सम्मत जली।सब सूना-सूना। पन्द्रह दिन पहले से होली इकट्ठा करने का उत्साह नदारद रहा। एक समय था जब हम बच्चों के साथ गांव के बड़े भी बच्चे बन जाते थे।एक गांव के शातिर दूसरे गांव की सम्मत चुराने की जुगत भिड़ाते रहते थे। इसके लिए समर भी सजते थे। पर बाद में सब फाग गीतों की रसध्वनि मे घुल मिल कर अमिय हो जाता।पंचगोइठी मांगने वालों की ठिठोली। बसंत पंचमी से ढोल मंजीरों की संगीत पर फगुहाऱों के पंचम सुर टटकी आयी दूल्हन के मन को रागरस में विभोर कर देते थे। जिनके प्रियतम इस फागुन घर नहीं आ पाये उन विरहनियों के कोकिल कण्ठ से फूट पड़ता था
"फागुन मास कटै कइसे सजनी,
नहिं आए बालम घर मोर
केहि संग खेलौं होरी ।।
रंग पाल, द्विज छोटकुन, कवि सूरदास जैसे कवियों चौपाल,तिताल,घमार,बारह मासा,उलारा के साथ साथ दूसरे बासंती रागों में पिरोये गये प्रेम, भक्ति, देश प्रेम सहित अन्यान्य भावों के फगुआ गीतों से गांव मस्त रहता।
"एहि द्वारे मंगलवार होरी होरी है।"
के गगन भेदी आलाप में यह तय कर पान कठिन था कि कौन से स्वर शत्रु के हैं और कौन मित्र के ।
मोहन धरि रूप जनाना,
बेचन चले चुड़िया सहाना,
नगर बरिसाना
तिरलोकी तिवारी साधना तिवारी और हंसू हरिजन के समवेत स्वरों से सहकार करती चच्चा गुलचम्मन खलीफा के ढ़ोल की थाप से अलौकिक संगीत का ऐसा समा बंध जाता कि आम की मंजरी मंजरी नाच पड़ती।उसके भावावेग में ऊच-नीच,जाति-पाति धर्म-सम्प्रदाय की बंदिशें ऐसे ढ़ह जातीं जैसे नदी के प्रबल वेग में कच्चे मकान।
पर मेरा मन आज फिर निराश है।देख रहा हूं समाज कैसे बदल रहा है। मातृभाषा भोजपुरी का चीरहरण करते अश्रव्य तुकबंदियों पर शराब के नशे में कैसे नाच रहा है हमारा युवा।होश नहीं है उसे कि कहां जा रहा है वह।
यह बदलाव नहीं है। ध्वंस का आरम्भ है।ऐसा ही चलता रहा तो हम कहां पहुंचेंगे?पता नहीं। हमें बाजार नीत तथाकथित आधुनिक सभ्यता से कुछ ज्यादा सावधानी से गले मिलना होगा।ये लोक पर्व हमारी पहचान हैं। इनकी पारम्परिक संरचना बचाना हमारा सांस्कृतिक ही नहीं राष्ट्रीय कर्तव्य भी है।हमें अपनी युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना होगा। जड़ टूटा पादप कभी जीवित नहीं बचता।
आचार्य ओमप्रकाश मणि
What's Your Reaction?